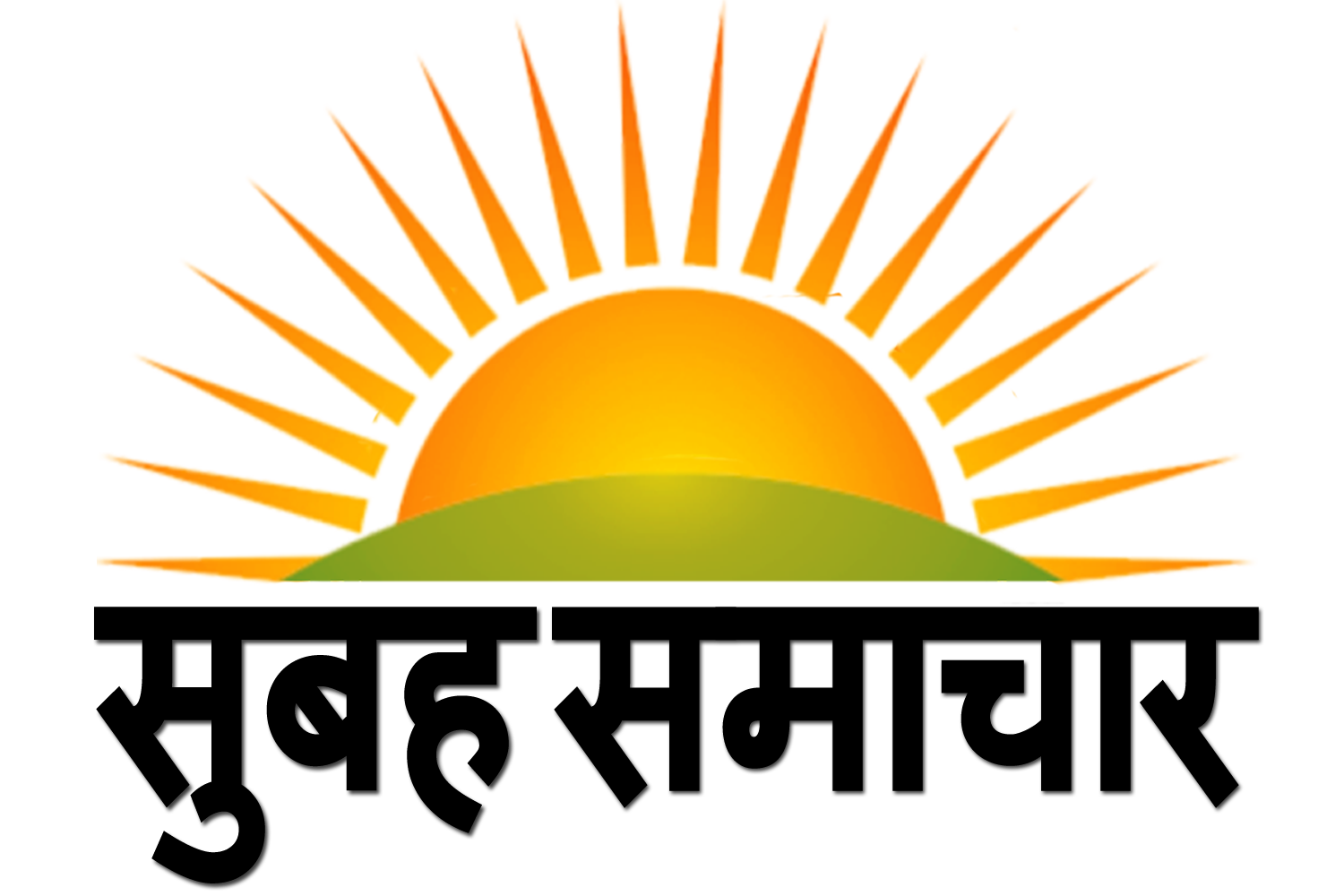एक इतिहासकार की बात: शोध करने वाला पांच साल से जेल में, हमारे जीवन की दिशाएं इतनी अलग क्यों हो गईं?
एक पीएचडी स्कॉलर का शोध ब्रिटिश काल के अधीन सिंहभूम क्षेत्र के आदिवासी समाज के जीवन में हुए परिवर्तन पर केंद्रित है, जो यह बताता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह क्षेत्र में सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण हासिल किया। साथ ही इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे उपनिवेशवाद ने सिंहभूम के प्राकृतिक परिदृश्य, कानूनी, आर्थिक व राजनीतिक ढांचे में आमूलचूल बदलाव किया। अध्ययन के दायरे में उपनिवेशी वन नीति का व्यावसायिक झुकाव, गांव के मुखियाओं की बदलती स्थिति, जिन्हें नए शासन से सामंजस्य स्थापित करना पड़ा और आदिवासी समुदायों की वे प्रतिक्रियाएं शामिल हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में आए गहरे परिवर्तन के बाद व्यक्त कीं। पर्यावरण, समाज और राजनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए शोधकर्ता ने बौद्धिक इतिहास की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम किया है। यूरोपीय अधिकारियों और भारतीय मानव विज्ञानियों द्वारा सिंहभूम के आदिवासियों पर लिखे ग्रंथों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। इस नए इतिहासकार के शोध कार्य में छह प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जिनका मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं। पहली, आदिवासियों के साहित्य पर शोधकर्ता की अच्छी पकड़ है। पूर्ववर्ती लेखकों में चाहे वे मशहूर हैं या नहीं, उन्होंने गहन अध्ययन किया है। झारखंड की जनजातियों से लेकर भारत के अन्य क्षेत्र की जनजातियों पर शानदार काम किया है। दूसरी, प्राइमरी डेटा की विविधता का व्यापक उपयोग शोधकर्ता ने किया है। यह शोध राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के अभिलेखागारों में की गई गहन खोजबीन से गुजरता है। साथ ही ऐसे लेखों और पुस्तकों पर भी प्रकाश डालता है, जो 100 साल पहले प्रकाशित हुई थीं और जिनके बारे में अब बहुत कम लोग जानते हैं। तीसरी विशेषता यह कि शोधार्थी महान फ्रांसीसी इतिहासकार मार्क ब्लोच के इस कथन को मानो आत्मसात कर चुका है कि “एक इतिहासकार को मोटी नोटबुक के साथ-साथ मोटे जूते की भी आवश्यकता होती है।” चौथी, अपने तर्क स्पष्ट करने के लिए शोधार्थी ने प्राइमरी डाटा से सजीव उद्धरण चुने हैं। उदाहरण के लिए, 19वीं शताब्दी के एक ब्रिटिश अधिकारी का यह उद्धरण देखें, जो जंगल में हुए शिकार का वर्णन करते हुए आदिवासी जीवन की रंगीन छवि प्रस्तुत करता है- “यहां हैं नाचते-गाते संथाल, फूलों और पंखों से सजे हुए, जिनकी बांसुरियां पिथ से बनी झालरों से अलंकृत हैं, लुकिसिनी पहाड़ियों के जंगली कुरिया (पहाड़ी लोग), कुर्मी, तांती सुंदी, ग्वाला आदि सब अपने मधुर ध्वनियों वाले वाद्य यंत्रों के साथ तलवारों, कुल्हाड़ियों और तरह-तरह के धनुष-बाणों से लैस और लोग सादे, सरल, पर सबसे भारी शिकार बैगों के साथ। इसी तरह एक सदी पहले का उद्धरण (अभिलेखागार में संरक्षित एक दस्तावेज से लिया गया है) प्रस्तुत है, जो असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले एक व्यक्ति के कथन का अनुवाद है- “अब स्वराज आ गया है और गांधी उसके प्रमुख हैं। अंग्रेज देश छोड़ रहे हैं और चाईबासा के कुछ अंग्रेज तीन-चार महीनों में भाग जाएंगे। गांधी महात्मा एक स्कूल खोलेंगे और सरकार के स्कूल नष्ट कर दिए जाएंगे। गांधी के स्कूल में कोई फीस नहीं दी जाएगी। पांचवीं, पीएचडी स्कॉलर ने अपने शोध को सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। एकेडमिक शब्दों की संख्या कम है। छठी विशेषता यह कि पीएचडी स्कॉलर ने अपने तर्कों को सूक्ष्मता और गहराई से प्रस्तुत किया है। इस बात का खास ख्याल रखा है कि अंग्रेज अधिकारियों और उनके समकालीनों ने आदिवासी जीवन की रूढ़ छवियों को जिस तरह गढ़ा, उसका दोहराव न हो। उन लेखकों की आलोचना की है, जो यह मानते हैं कि उपनिवेशकालीन और समकालीन आदिवासी आंदोलनों के बीच सीधी रेखा खींची जा सकती है, जैसे आंदोलन आधुनिक राज्य द्वारा पूर्ववर्ती आदर्श और परंपरागत समाज के विघटन से प्रेरित हुए हों। शोधकर्ता के अनुसार, ऐसे लेखन आदिवासियों को एकरूप और अपरिवर्तनीय परंपराओं पर आधारित समुदाय के रूप में प्रस्तुत करने की भूल करते हैं। शोध दिखाता है कि जहां बहुत से आदिवासी राज्य के अतिक्रमण का विरोध करते हैं, वहीं उनके कुछ समूह राज्य के साथ सहयोग भी करते हैं और कुछ अपने समुदायों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बातचीत और समझौते की राह भी चलते हैं। हालांकि शोध में कुछ कमियां भी हैं। शोधार्थी ने कुछ महत्वपूर्ण सेकंडरी डेटा की अनदेखी की है, जो विषय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। मसलन, भारतीय मानव विज्ञान के इतिहास पर टीएन मदान के लेखन का संज्ञान नहीं लिया गया। मुझे लगता है, लोक कथाओं और मौखिक इतिहास का उपयोग अधिक किया होता तो शोध और समृद्ध हो सकता था। प्राइमरी डेटा के सभी उद्धरण इतने प्रभावशाली नहीं थे, जितने कि कुछ उदाहरण मैंने यहां बताएं हैं। कुछ इतने लंबे हैं कि उन्होंने बात को हल्का कर दिया है। इसके बावजूद यह उन सर्वश्रेष्ठ भारतीय डॉक्टरेट शोध प्रबंधों में से एक है, जिन्हें मैंने अभी तक पढ़ा है। आम तौर पर इस स्तर का शोध कुछ साल में कुशल संपादक द्वारा कमियां दूर करने के बाद पुस्तक रूप में प्रकाशित हो जाता है। पर्यावरण और सामाजिक इतिहास के काम में नंदिनी सुंदर की सबाल्टर्न एंड सोवरनस और महेश रंगराजन की फेंसिंग द फॉरेस्ट में पाएंगे कि इन शोध प्रबंधों की प्रस्तुति और पुस्तक प्रकाशन के बीच बहुत कम समय का अंतर रहा। यह सिलसिला हाल के वर्षों में प्रकाशित भवानी रामन, आदित्य बालसुब्रमण्यम, निखिल मेनन और दिन्यार पटेल के कामों में भी दिखता है, जिनके काम की शुरुआत भी डॉक्टरेट शोध प्रबंध के रूप में हुई थी। इन किताबों को व्यापक रूप से पढ़ा और सराहा गया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस शोध प्रबंध की मैं चर्चा कर रहा हूं, वह भी पुस्तक के रूप में आने पर ऐसी ही प्रशंसा प्राप्त करे। यह शोध प्रबंध 2018 में प्रस्तुत किया गया था, पर अब तक किताब के रूप में प्रकाशित नहीं हो सका है। शोध करने वाले का नाम उमर खालिद है। यह इतिहासकार पांच वर्षों से अधिक समय से बिना जमानत जेल में है। मेरी कभी डॉ. उमर खालिद से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन दिसंबर 2019 के एक दिन हम दोनों ने देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। वह दिल्ली में और मैं बंगलूरू में था। तब से इन वर्षों में मैंने अक्सर सोचा है कि हमारे जीवन की दिशाएं इतनी अलग क्यों हो गईं
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 02, 2025, 08:04 IST
एक इतिहासकार की बात: शोध करने वाला पांच साल से जेल में, हमारे जीवन की दिशाएं इतनी अलग क्यों हो गईं? #Opinion #National #SubahSamachar