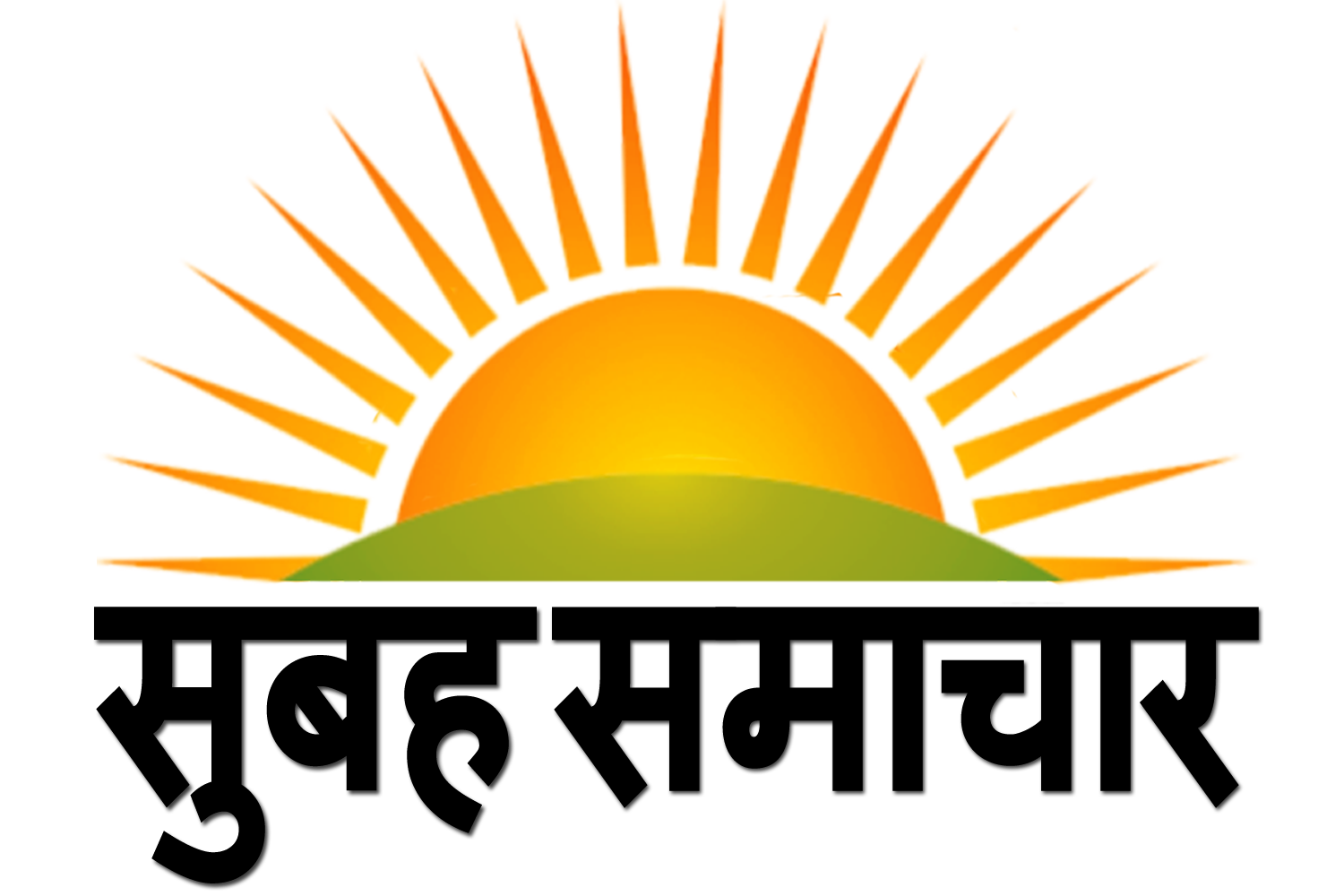जातिगत गणना : असल समस्या तो अब शुरू होगी, राह में आएगी सामाजिक और विभाजक शक्तियों की दीवार
वर्ष 1965 में पाकिस्तानी हमले के खिलाफ देशवासियों को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक वक्त का भोजन त्याग के साथ जय जवान जय किसान का अमर नारा दिया था, लेकिन पहलगाम में पाकिस्तानी हमले के बाद पक्ष-विपक्ष के नेता धर्म और जाति के वोट बैंक की सियासत में मग्न हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अप्रैल, 2021 में जनगणना में जातियों का डाटा इकट्ठा करने की बात सरकार से कही थी, लेकिन जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि जातिगत जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। उसके बाद नवंबर, 2023 में विकसित भारत की संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब, महिला, किसान और युवा चार जातियों का जिक्र किया था। प्रवासी श्रमिकों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने भारत में गरीबों की बढ़ती आबादी पर हैरानी जताई है। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति से भारत में धर्म और जातियों के विभाजन को बढ़ावा दिया था। साल 1901 की जनगणना में 1,646 और साल 1931 की जनगणना में कुल 4,147 जातियों की संख्या बताई गई थी। साल 1931 की जनगणना के अनुसार, 52.4 फीसदी ओबीसी, 22.6 फीसदी अनुसूचित जाति/जनजाति, 17.6 फीसदी अगड़ी जातियां और 16.2 फीसदी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट अविभाजित भारत के 50 साल पुराने इन्हीं आंकड़ों पर आधारित थी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे से वोट बैंक की फसल अच्छी कटती है, इसलिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सभी दलों के नेता उत्साहपूर्ण तरीके से सहमत हैं। यूपीए सरकार के दौरान साल 2011 में जनगणना के बाद सामाजिक और आर्थिक नजरिये से जातियों की गणना हुई थी। कई रिपोर्टों के अनुसार, उस सर्वे में 46 लाख से ज्यादा जातियों का विवरण था। इसलिए वह रिपोर्ट पूरे तौर पर कभी प्रकाशित ही नहीं हुई। जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय लिस्ट में लगभग 2,633, जबकि राज्यों में लगभग 3,651 ओबीसी जातियां शामिल हैं। केंद्र सरकार मोबाइल और एप के माध्यम से डिजिटल जनगणना कराने का दावा कर रही है। 2011 की जनगणना में लगभग 25 लाख सरकारी शिक्षकों और कर्मियों की ड्यूटी के साथ लगभग 2,200 करोड़ रुपये का खर्च हुए थे। साल 2019 में जनगणना के मद में लगभग 8,754 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान था, जो अब बढ़ गया होगा। उसके बावजूद 2025-26 के बजट में जनगणना के मद में केंद्र सरकार ने सिर्फ 574 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। 16वीं जनगणना के लिए निर्धारित फॉर्म में बीसवां नया कॉलम बढ़ाने और 2011 की अप्रकाशित रिपोर्ट की गलतियों से बचने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर जातियों व उपजातियों की लिस्ट को अंतिम रूप देना होगा। इस प्रक्रिया में विपक्ष शासित राज्यों से समुचित विमर्श से जाति के नाम पर सामाजिक असंतोष को भड़काने वाली ताकतों को नियंत्रित रखना बड़ी चुनौती होगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईडब्ल्यूएस के साथ कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है। जनगणना में मुस्लिम समुदाय में जातियां के सर्वे पर भी कानूनी विवाद हो सकते हैं। सरकार की तरफ से सशक्तीकरण और समावेशी विकास के दावे किए जा रहे हैं, पर इसे सफल बनाने के लिए सरकार को चार बड़ी सांविधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, पहला-संविधान में आबादी के अनुसार विधायकों और सांसदों की सीटों का निर्धारण होता है, जिसे परिसीमन कहते हैं। दक्षिण के राज्य 1971 की पुरानी आबादी के अनुसार परिसीमन की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। परिसीमन पर क्षेत्र और भाषा के आधार पर विवाद को रोकने के लिए सरकार जनगणना के फैसले को टाल रही है। उस फॉर्मूले के अनुसार, जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने में भी विलंब हो सकता है। दूसरा-संविधान के 106वें संशोधन से विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण मिला था। सुप्रीम कोर्ट की महिला जज और संभावित आगामी चीफ जस्टिस बीवी नागरत्ना ने महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग दोहराई है। सरकारी दावों के अनुसार, यदि 2026 में जनगणना पूरी हो गई, तो 2029 के आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने का दबाव बढ़ेगा। अब जाति जनगणना की नई गुगली के बाद महिला आरक्षण में भी जातिगत आरक्षण की मांग बढ़ सकती है। ऐसा होने पर संविधान में नए सिरे से संशोधन करना होगा। तीसरा-संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, जनगणना का विषय केंद्र सरकार के अधीन आता है। आजादी के बाद साल 1951 की पहली जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजातियों का ही विवरण लिया गया था। उसके बाद साल 1961 में राज्य सरकारों को ओबीसी जातियों के सर्वेक्षण की इजाजत मिली थी। बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कनार्टक ने सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सामाजिक, आर्थिक सर्वे की आड़ में जातिगत जनगणना की, जिसके लिए संविधान में इजाजत नहीं है। भविष्य में ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार कानून में बदलाव की पहल कर सकती है। चौथा-संविधान के अनुच्छेद-15 में धर्म, जाति, लिंग, भाषा और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित है, लेकिन शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के अपवाद के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। जाति के आधार पर आरक्षण को सरकारी मान्यता मिलने से संविधान में समानता के मौलिक अधिकार का संस्थागत और संगठित उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी फैसले में आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50 फीसदी निर्धारित किया था। जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार और विपक्ष संविधान संशोधन पर सहमत हो सकते हैं, जिससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों से बड़ी संविधान पीठ का गठन करना होगा, जिसका फैसला केशवानंद भारती मामले से भी ज्यादा ऐतिहासिक हो सकता है। क्या बिहार चुनाव के पहले जाति गणना की घोषणा पर प्रशासनिक तौर पर अमल होगा या यह आगे खिसक सकता है जाति गणना की सियासत से विभाजक शक्तियां प्रबल होंगी, जिससे गरीबी और असमानता का संकट बढ़ने के साथ टेक और एआई के युग में भारत अपनी जनसांख्यिकी के लाभ से वंचित रह सकता है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 02, 2025, 07:01 IST
जातिगत गणना : असल समस्या तो अब शुरू होगी, राह में आएगी सामाजिक और विभाजक शक्तियों की दीवार #Opinion #National #SubahSamachar